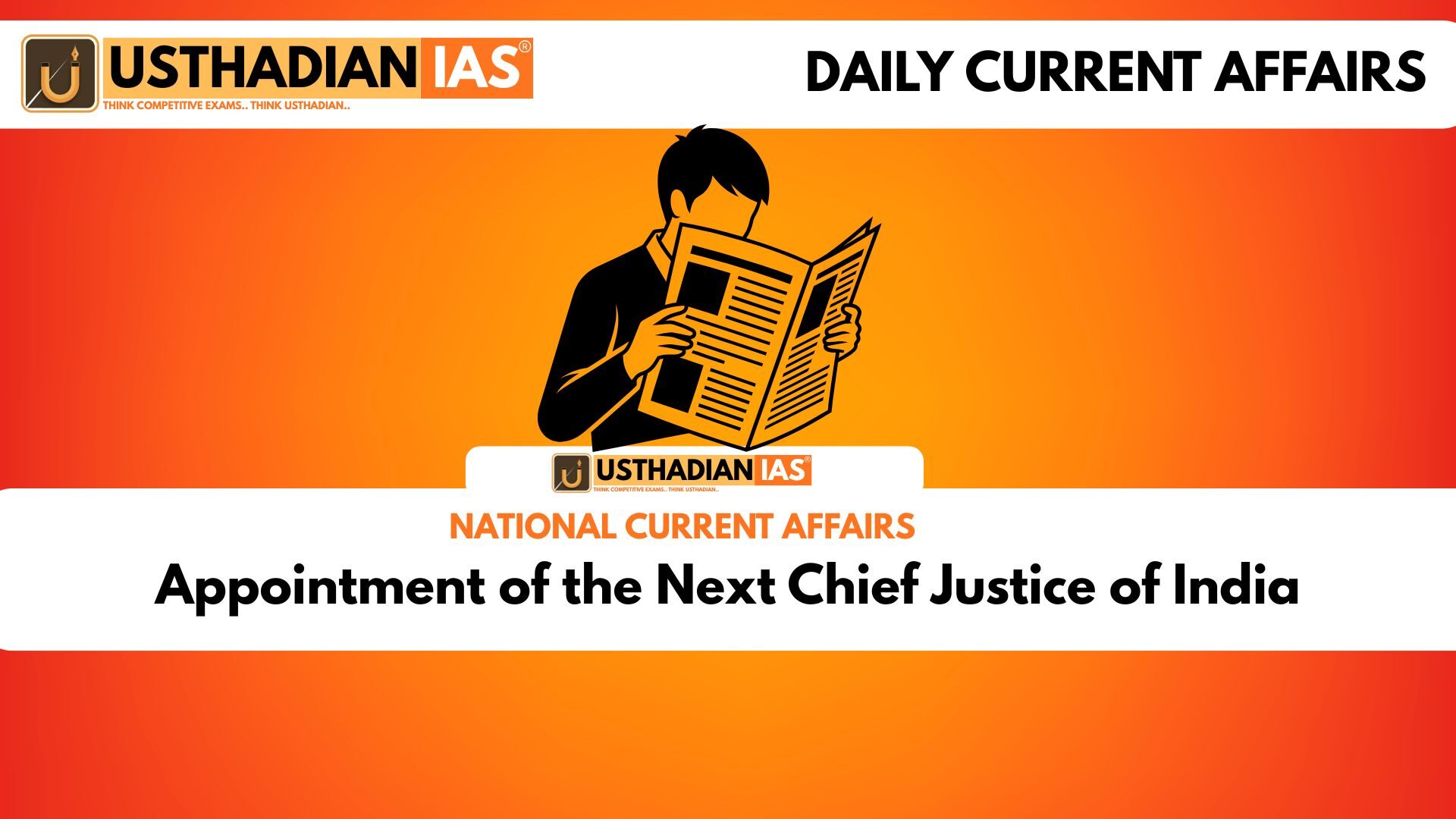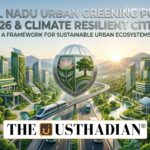भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रक्रिया
मुख्य न्यायाधीश (CJI) की नियुक्ति एक निर्धारित परंपरा के अनुसार की जाती है, जो संविधान के अनुच्छेद 124(2) और प्रक्रिया ज्ञापन (Memorandum of Procedure – MoP) में निहित है।
केंद्र सरकार, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति से लगभग एक माह पूर्व, उनसे उनके उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करने का अनुरोध करती है।
आमतौर पर, वरिष्ठता सिद्धांत (Seniority Principle) का पालन किया जाता है, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है।
वर्तमान सीजेआई अपने उत्तराधिकारी का नाम विधि और न्याय मंत्रालय को भेजते हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री की स्वीकृति प्राप्त होने पर भारत के राष्ट्रपति नियुक्ति की आधिकारिक अधिसूचना (Warrant of Appointment) जारी करते हैं।
स्थैतिक जीके तथ्य: भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद 26 जनवरी 1950 को स्थापित हुआ था, और पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच. जे. कनिया थे।
सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति
मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम प्रणाली की अनुशंसा पर की जाती है।
कॉलेजियम प्रणाली में CJI और सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।
यह प्रणाली तीन ऐतिहासिक न्यायिक मामलों (1981, 1993, 1998) के माध्यम से विकसित हुई, जिन्होंने सामूहिक रूप से न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया को पुनर्परिभाषित किया।
इसी प्रकार, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत की जाती है, जहाँ कॉलेजियम में CJI और सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं।
कॉलेजियम की अनुशंसाएँ विधि मंत्रालय को भेजी जाती हैं, फिर प्रधानमंत्री को अग्रेषित की जाती हैं, और अंततः राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत की जाती हैं।
स्थैतिक जीके टिप: सर्वोच्च न्यायालय की अनुमोदित शक्ति 34 न्यायाधीशों (CJI सहित) की है।
कॉलेजियम प्रणाली से जुड़ी चिंताएँ
कॉलेजियम प्रणाली पर पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी को लेकर लगातार आलोचनाएँ होती रही हैं।
निर्णय प्रक्रिया गोपनीय रहती है, और चयन या अस्वीकृति के पीछे के कारण सार्वजनिक रूप से साझा नहीं किए जाते।
इसके अलावा, समीक्षा की कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं है, जिससे पक्षपात या नियंत्रण संतुलन की कमी की धारणा बनती है।
एक अन्य चिंता यह है कि इस प्रणाली में कार्यपालिका की भूमिका सीमित हो जाती है, और अंतिम निर्णय मुख्यतः न्यायपालिका के पास रहता है, जिससे शक्ति पृथक्करण (Separation of Powers) पर बहस उठती है।
NJAC और 99वाँ संविधान संशोधन
इन मुद्दों को दूर करने के लिए संसद ने 2014 में 99वाँ संविधान संशोधन और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम पारित किया।
NJAC का उद्देश्य न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल कर संतुलित भागीदारी सुनिश्चित करना था।
हालाँकि, 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने NJAC को असंवैधानिक घोषित कर दिया — जिसे चौथे न्यायाधीश मामले (Fourth Judges Case) के रूप में जाना जाता है — और कॉलेजियम प्रणाली को पुनः स्थापित किया।
इस ऐतिहासिक निर्णय ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भारत के मौलिक ढाँचे (Basic Structure) का हिस्सा घोषित किया।
स्थैतिक जीके तथ्य: NJAC में CJI, दो वरिष्ठतम न्यायाधीश, विधि मंत्री, और दो विशिष्ट व्यक्ति (Eminent Persons) शामिल होने का प्रस्ताव था।
स्थैतिक उस्तादियन करंट अफेयर्स तालिका
| विषय (Topic) | विवरण (Detail) |
| संवैधानिक अनुच्छेद (न्यायाधीश नियुक्ति) | अनुच्छेद 124(2) |
| नियुक्ति प्राधिकारी | भारत के राष्ट्रपति |
| CJI चयन का पारंपरिक आधार | वरिष्ठता सिद्धांत (Seniority Principle) |
| मुख्य सलाहकारी निकाय | कॉलेजियम प्रणाली |
| कॉलेजियम संरचना | CJI + 4 वरिष्ठतम सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश |
| कॉलेजियम प्रणाली की उत्पत्ति | तीन न्यायाधीश मामले (1981, 1993, 1998) |
| NJAC अधिनियम और 99वाँ संशोधन | 2014 में पारित, 2015 में निरस्त |
| भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश | न्यायमूर्ति एच. जे. कनिया |
| सर्वोच्च न्यायालय की अनुमोदित शक्ति | 34 न्यायाधीश (CJI सहित) |
| चौथे न्यायाधीश मामले में स्थापित सिद्धांत | न्यायिक स्वतंत्रता – संविधान की मूल संरचना का हिस्सा |