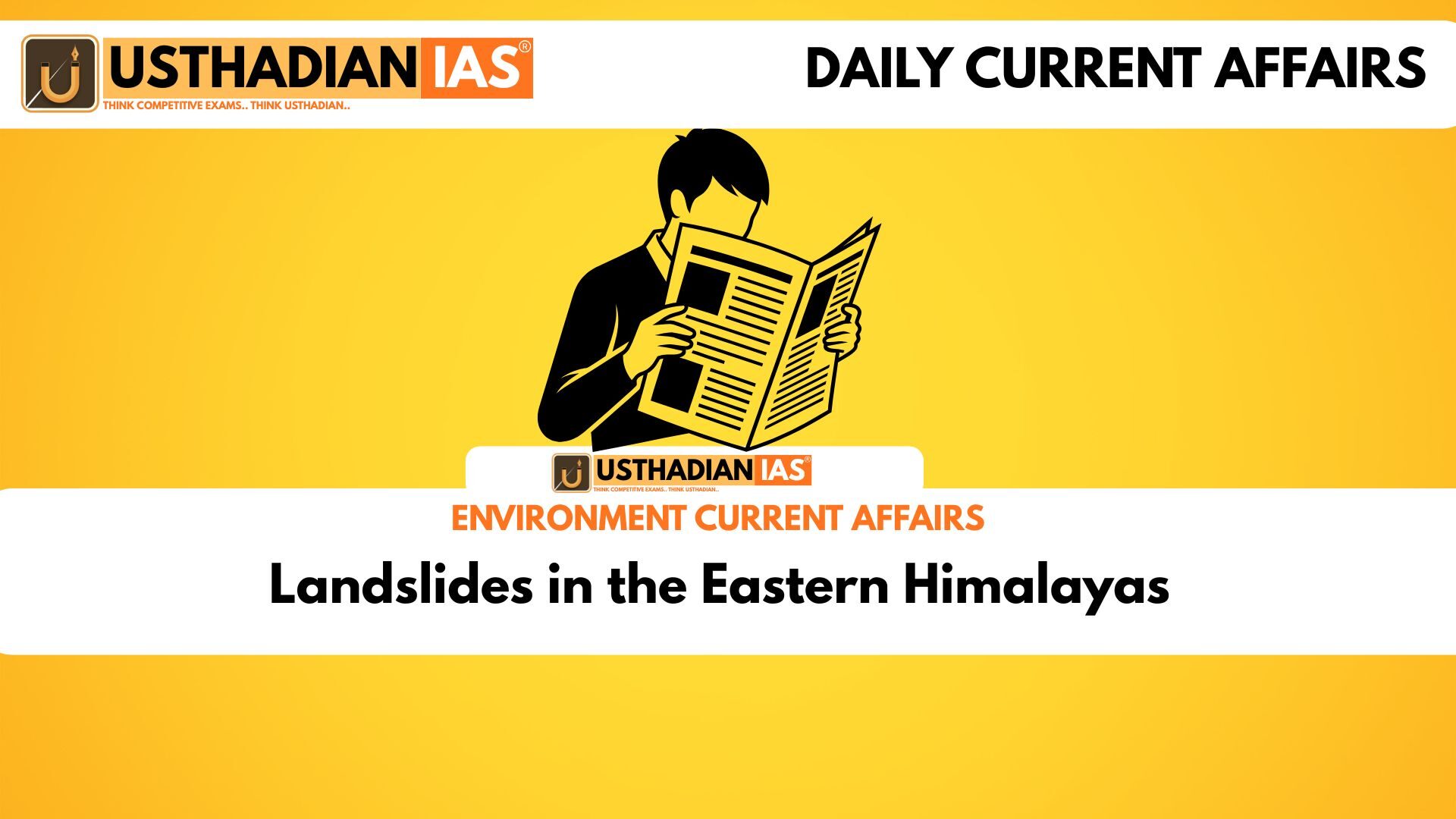भूस्खलन को समझना
भूस्खलन (Landslide) वह प्रक्रिया है जिसमें चट्टान, मिट्टी और मलबा गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से नीचे की ओर खिसकता है।
भारत इस प्राकृतिक आपदा के लिए अत्यधिक संवेदनशील देशों में से एक है।
ISRO लैंडस्लाइड एटलस 2023 के अनुसार, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.6% भाग भूस्खलन के प्रति संवेदनशील है।
इसमें से तीन-चौथाई से अधिक भाग हिमालयी क्षेत्र में आता है, जो इसे विश्व के सबसे अस्थिर भूभागों में से एक बनाता है।
स्थैतिक सामान्य ज्ञान तथ्य: हिमालय विश्व की सबसे युवा मोड़ पर्वत श्रृंखला (Fold Mountains) है, जिसका निर्माण लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले हुआ था।
पूर्वी हिमालय की संवेदनशीलता
हाल ही में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिलों में हुए भूस्खलनों ने पूर्वी हिमालय की नाजुकता को उजागर किया है।
इन क्षेत्रों में प्राकृतिक और मानवजनित दोनों कारणों से बार-बार भूस्खलन होता है।
लगातार मानसूनी वर्षा, मिट्टी में अधिक नमी, और अस्थिर ढलानें जब निर्माण, सड़क कटाई और वनों की कटाई जैसी मानवीय गतिविधियों के साथ मिलती हैं, तो आपदा की आवृत्ति बढ़ जाती है।
स्थैतिक सामान्य ज्ञान टिप: दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, भारत के सबसे भूस्खलन-प्रवण क्षेत्रों में से होकर गुजरती है।
भूस्खलन के प्राकृतिक कारण
हिमालय का निर्माण भारतीय और यूरेशियाई प्लेटों की टक्कर से हुआ, जिससे दरारों और भ्रंशों से भरी चट्टानें बनीं।
यह भूकंपीय अस्थिरता ढलानों को कमजोर बनाती है।
मुख्य प्राकृतिक कारण —
• भारी वर्षा और क्लाउडबर्स्ट मिट्टी को संतृप्त करते हैं और ढलान खिसकने का कारण बनते हैं।
• हिमपात के पिघलने और आकस्मिक बाढ़ों से अस्थिर भूभाग और कमजोर हो जाता है।
• भूकंपीय गतिविधियाँ पहले से कमजोर क्षेत्रों में अतिरिक्त जोखिम जोड़ती हैं।
• जलवायु परिवर्तन के कारण चरम मौसम की घटनाएँ बढ़ रही हैं, जिससे भूस्खलन की आवृत्ति भी बढ़ गई है।
मानव-जनित कारण
मानव गतिविधियाँ प्राकृतिक जोखिम को और बढ़ा देती हैं।
• अनियोजित शहरी विस्तार और बड़े अवसंरचनात्मक प्रोजेक्ट पहाड़ियों की स्थिरता को कमजोर करते हैं।
• सड़क निर्माण, सुरंग खुदाई और खनन से पर्वतीय ढलानें कमजोर पड़ जाती हैं।
• वनों की कटाई और खनन गतिविधियाँ प्राकृतिक जल निकासी प्रणाली को बाधित करती हैं।
• संवेदनशील क्षेत्रों में अतिक्रमण स्थानीय समुदायों के लिए आपदा का जोखिम बढ़ाता है।
स्थैतिक सामान्य ज्ञान तथ्य: हिमालयी क्षेत्र भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 16.2% हिस्सा है और यह 13 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है।
भूस्खलन प्रबंधन पर एनडीएमए के दिशानिर्देश
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने भूस्खलन जोखिमों को कम करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं —
• संवेदनशील क्षेत्रों का जोखिम और भेद्यता मानचित्रण (Risk & Vulnerability Mapping)।
• बहु-आपदा योजना (Multi-hazard Planning) जिसमें भूकंप, बाढ़ और हिमस्खलन के साथ भूस्खलन को भी शामिल किया गया है।
• प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (Early Warning System) से उच्च जोखिम वाले ढलानों की निगरानी।
• आपात प्रतिक्रिया तंत्र (Emergency Response Mechanisms) जिसमें NDRF, अर्धसैनिक बलों और स्थानीय एजेंसियों की भागीदारी।
• क्षमता निर्माण और जन-जागरूकता कार्यक्रम ताकि समुदाय स्वयं-सुरक्षा उपाय सीख सकें।
• सख्त भूमि उपयोग और ढलान प्रबंधन के लिए कानूनी ढांचा।
स्थैतिक सामान्य ज्ञान टिप: NDMA की स्थापना 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम (Disaster Management Act) के अंतर्गत की गई थी, और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।
आगे की दिशा
पूर्वी हिमालय में भूस्खलन जोखिम को कम करने के लिए वैज्ञानिक निगरानी, सतत भूमि उपयोग और सख्त पर्यावरणीय नियंत्रण आवश्यक हैं।
इंजीनियरिंग उपायों, सामुदायिक भागीदारी और रियल-टाइम डेटा मॉनिटरिंग को एकीकृत करके ही संवेदनशील आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।
स्थैतिक उस्तादियन करंट अफेयर्स तालिका
| विषय | विवरण |
| हालिया घटना | दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिलों में भूस्खलन |
| भारत की संवेदनशीलता | 12.6% भूमि क्षेत्र भूस्खलन के प्रति संवेदनशील |
| उच्च जोखिम क्षेत्र | हिमालयी क्षेत्र, जिसमें 75% से अधिक जोखिम केंद्रित है |
| भूवैज्ञानिक कारण | भारतीय और यूरेशियाई प्लेटों की टक्कर |
| जलवायु संबंध | जलवायु परिवर्तन से वर्षा और चरम घटनाओं में वृद्धि |
| मानव कारण | सड़क निर्माण, सुरंग खुदाई, वनों की कटाई, खनन, शहरीकरण |
| NDMA की भूमिका | जोखिम मानचित्रण, चेतावनी प्रणाली, आपदा तैयारी दिशानिर्देश |
| प्रमुख बल | राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) |
| स्थैतिक सामान्य ज्ञान | हिमालय विश्व की सबसे युवा मोड़ पर्वत श्रृंखला है |
| NDMA स्थापना वर्ष | 2005 (आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत) |