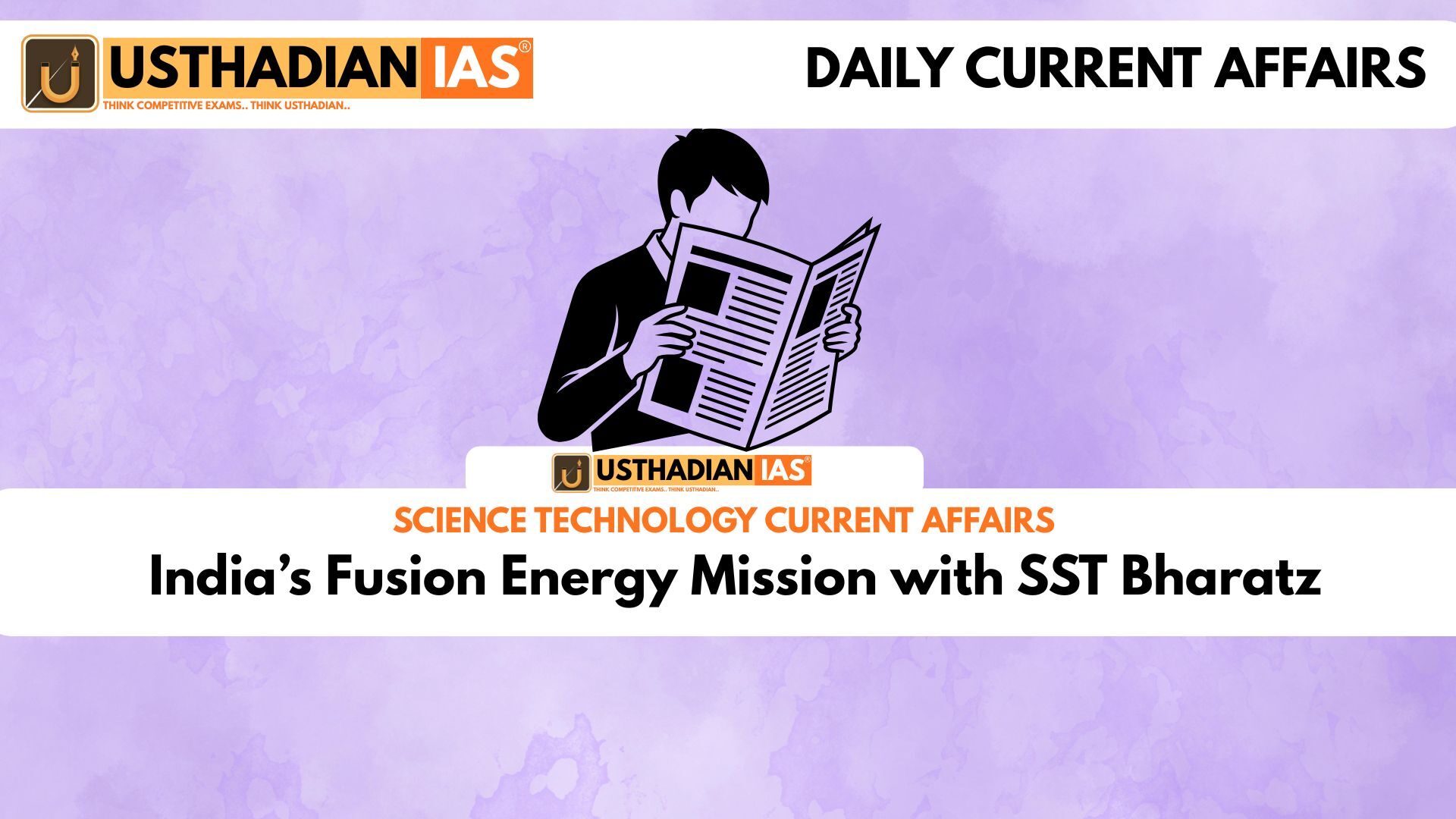भविष्य की ऊर्जा स्रोत के रूप में फ्यूज़न
फ्यूज़न ऊर्जा दो हल्के नाभिकों को जोड़कर अपार ऊर्जा उत्पन्न करती है – यही प्रक्रिया तारों को शक्ति देती है। यह परमाणु विखंडन की तुलना में स्वच्छ और सुरक्षित विकल्प है। फ्यूज़न में बहुत कम रेडियोधर्मी अपशिष्ट उत्पन्न होता है और दीर्घकालिक भंडारण की समस्या घट जाती है। लेकिन इसके लिए अत्यधिक परिस्थितियों की ज़रूरत होती है, जिनमें 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान शामिल है।
स्थैतिक तथ्य: पहला नियंत्रित फ्यूज़न प्रयोग 1958 में सोवियत संघ में टोकामक तकनीक से सफल हुआ था।
भारत का टोकामक विकास पथ
भारत का फ्यूज़न शोध चुंबकीय नियंत्रण (Magnetic Confinement) पर आधारित है। वर्तमान SST-1 टोकामक 650 मिलीसेकंड तक प्लाज़्मा को नियंत्रित कर सकता है, जबकि लक्ष्य 16 मिनट का है। आने वाला SST-भारत रिएक्टर एक फ्यूज़न-विखंडन हाइब्रिड होगा, जो 130 मेगावॉट बिजली उत्पन्न करेगा (100 मेगावॉट विखंडन से, 30 मेगावॉट फ्यूज़न से)। वर्ष 2060 तक 250 मेगावॉट का पूर्ण प्रदर्शन रिएक्टर तैयार करने की योजना है, जिसका आउटपुट-टू-इनपुट अनुपात 20 होगा।
स्थैतिक तथ्य: “Tokamak” शब्द रूसी भाषा से आया है, जिसका अर्थ है “Toroidal Chamber with Magnetic Coils।”
वैश्विक परियोजनाएँ और भारत की सतर्क समयसीमा
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई देश तेज़ प्रोटोटाइप विकसित कर रहे हैं। यूके का STEP कार्यक्रम 2040 तक प्रोटोटाइप तैयार करने का लक्ष्य रखता है। अमेरिका की कई निजी कंपनियाँ 2030 के दशक तक वाणिज्यिक संयंत्र शुरू करने की ओर बढ़ रही हैं। चीन का EAST टोकामक 1,000 सेकंड से अधिक प्लाज़्मा अवधि का रिकॉर्ड रखता है। भारत का 2060 लक्ष्य सतर्क लेकिन स्थिर दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें मज़बूत सार्वजनिक वित्त और अंतरराष्ट्रीय सहयोग शामिल है।
स्थैतिक तथ्य: ITER, विश्व की सबसे बड़ी फ्यूज़न प्रयोगशाला, कैडाराश (फ्रांस) में स्थित है और भारत इसका प्रमुख साझेदार है।
SST भारत के समर्थन में नवाचार
प्लाज़्मा अस्थिरता से निपटने के लिए डिजिटल ट्विन्स यानी वर्चुअल रिएक्टर विकसित किए जा रहे हैं, जो वास्तविक समय में प्लाज़्मा का अनुकरण करेंगे। मशीन लर्निंग का उपयोग नियंत्रण और दक्षता बढ़ाने के लिए होगा। विकिरण-रोधी सामग्रियों का विकास भी दीर्घकालिक संचालन हेतु आवश्यक है। इन नवाचारों का उद्देश्य लागत घटाना और प्रदर्शन सुधरना है, ताकि फ्यूज़न अधिक व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य हो सके।
आर्थिक और नीतिगत चुनौतियाँ
सबसे बड़ी चुनौती है आर्थिक व्यवहार्यता। फ्यूज़न शोध में भारी निवेश चाहिए, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा और परमाणु विखंडन संयंत्र पहले से ही भारत की ऊर्जा मिश्रण में प्रतिस्पर्धी हैं। अमेरिका और यूरोप की तरह भारत में निजी क्षेत्र की भागीदारी सीमित है। विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि फ्यूज़न की समयसीमाएँ अक्सर अधिक आशावादी होती हैं और लागत अभी भी अनिश्चित है।
स्थैतिक टिप: भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित हुआ था।
भारत के लिए रणनीतिक महत्व
भले ही वाणिज्यिक फ्यूज़न बिजली देर से आए, पर इसके वैज्ञानिक और रणनीतिक लाभ बहुत बड़े होंगे। सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट, प्लाज़्मा भौतिकी और सामग्री विज्ञान में प्रगति भारत के अनुसंधान ढाँचे को मज़बूत करेगी। ITER जैसी अंतरराष्ट्रीय साझेदारियाँ भारत की तकनीकी नींव और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ाएँगी।
Static Usthadian Current Affairs Table
| विषय | विवरण |
| SST-भारत रिएक्टर | 130 मेगावॉट उत्पादन वाला फ्यूज़न-विखंडन हाइब्रिड |
| प्रदर्शन लक्ष्य | 2060 तक 250 मेगावॉट रिएक्टर |
| वर्तमान टोकामक | SST-1, 650 मिलीसेकंड प्लाज़्मा अवधि |
| ITER का स्थान | कैडाराश, फ्रांस |
| यूके STEP कार्यक्रम | 2040 तक प्रोटोटाइप |
| चीन EAST | 1,000 सेकंड से अधिक प्लाज़्मा रिकॉर्ड |
| फ्यूज़न का लाभ | विखंडन से स्वच्छ, कम रेडियोधर्मी अपशिष्ट |
| भारत का पहला परमाणु संयंत्र | तारापुर, महाराष्ट्र (1969) |
| आवश्यक तापमान | 100 मिलियन °C से अधिक |
| आउटपुट-टू-इनपुट लक्ष्य | प्रदर्शन रिएक्टर में 20 अनुपात |