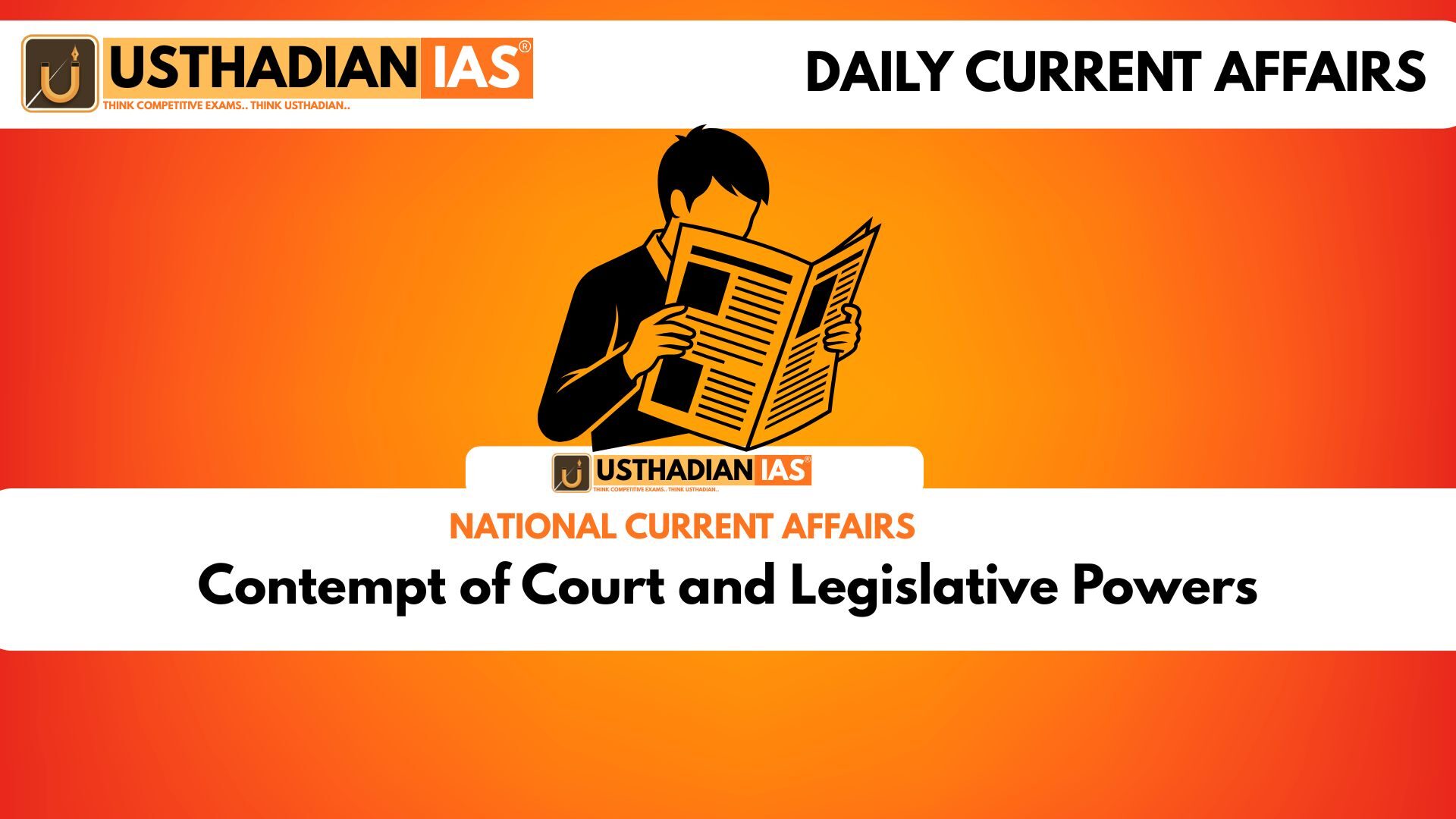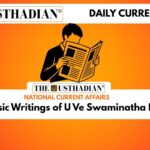न्यायपालिका और विधायिका के टकराव पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2025) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यदि कोई विधेयक या कानून किसी पुराने न्यायिक आदेश के खिलाफ जाता है, तो यह अदालत की अवमानना नहीं मानी जाएगी। यानी संसद या राज्य विधानसभा, किसी न्यायिक निर्णय का आधार हटाकर नया कानून बना सकती हैं, और यहां तक कि संविधान संशोधन के ज़रिए निरस्त किए गए कानून को पुनर्जीवित भी कर सकती हैं। यह न्यायपालिका और विधायिका की अलग–अलग भूमिकाओं और शक्तियों की पुष्टि करता है।
अदालत की अवमानना क्या है?
अदालत की अवमानना का अर्थ है – जानबूझकर अदालत के आदेश की अवहेलना करना, न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुँचाना या कार्यवाही में बाधा डालना। इसमें लिखित या मौखिक रूप से अदालत की छवि को नुकसान पहुँचाने वाले कार्य भी आते हैं।
विधायी आधार और कानूनी ढांचा
भारत में अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 यह निर्धारित करता है कि अवमानना क्या होती है और उसे कैसे निपटाया जाता है। 1975 में बनाए गए नियम, विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट में अवमानना मामलों की प्रक्रिया तय करते हैं।
अवमानना के प्रकार
- सिविल अवमानना: जब कोई व्यक्ति जानबूझकर अदालत के आदेश का पालन नहीं करता या अदालत से किए गए वादे को नहीं निभाता।
2. आपराधिक अवमानना: इसमें निम्नलिखित शामिल होते हैं:
- अदालत की छवि को नुकसान पहुँचाना या उसे बदनाम करना
- किसी लंबित कार्यवाही को प्रभावित करना
- न्याय की प्रक्रिया में बाधा डालना
कुछ अपवाद भी हैं
हर गलती को अवमानना नहीं माना जाता। कानून में कुछ रक्षात्मक उपाय भी हैं:
- न्यायालय की कार्यवाही की निष्पक्ष और सटीक रिपोर्टिंग की अनुमति है
- अनजाने में या भोलेपन से हुई अवमानना दंडनीय नहीं है
- न्यायिक फैसलों की उचित आलोचना भी दंडनीय नहीं है
अवमानना कानून से जुड़ी प्रमुख चिंताएँ
- बहुत अधिक लंबित मामले: सुप्रीम कोर्ट में 1,800 से अधिक और उच्च न्यायालयों में लगभग43 लाख अवमानना मामले लंबित हैं
- विवेकाधीन प्रयोग: अदालतें मामूली मामलों में भी कार्रवाई कर सकती हैं
- अस्पष्ट परिभाषाएँ: “कोर्ट को बदनाम करना” जैसे शब्द स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं हैं, जिससे दुरुपयोग की संभावना रहती है
संविधान में अवमानना से संबंधित प्रावधान
- अनुच्छेद 129: सुप्रीम कोर्ट को रिकॉर्ड कोर्ट माना गया है और उसे अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति दी गई है
- अनुच्छेद 215: उच्च न्यायालयों को भी ऐसी ही शक्ति प्रदान करता है
- अनुच्छेद 142: सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय देने के लिए आदेश पारित करने की शक्ति देता है
- अनुच्छेद 19(2): मुक्त भाषण के अधिकार पर अदालत की अवमानना जैसे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं
Static Usthadian Current Affairs Table
| विषय | विवरण |
| अदालत की अवमानना अधिनियम | 1971 में पारित, अवमानना की परिभाषा और सीमा निर्धारित करता है |
| सुप्रीम कोर्ट के नियम | 1975 से लागू, अवमानना की प्रक्रिया को विनियमित करते हैं |
| अवमानना के प्रकार | सिविल और आपराधिक अवमानना |
| सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 2025 | नंदिनी सुंदर केस – कानून आदेश के विरुद्ध हो तो अवमानना नहीं |
| अनुच्छेद 129 और 215 | सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों को अवमानना पर दंड देने की शक्ति |
| लंबित मामले | सुप्रीम कोर्ट में 1,800+, उच्च न्यायालयों में 1.43 लाख से अधिक |
| महत्वपूर्ण अपवाद | निष्पक्ष आलोचना और सटीक रिपोर्टिंग को अवमानना नहीं माना जाता |
| मौलिक अधिकार से संबंध | अनुच्छेद 19(1)(a) – अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, परंतु सीमाएं 19(2) में |
| रिकॉर्ड कोर्ट | ऐसी अदालत जिसके कार्य कानून और प्रमाण हेतु दर्ज किए जाते हैं |