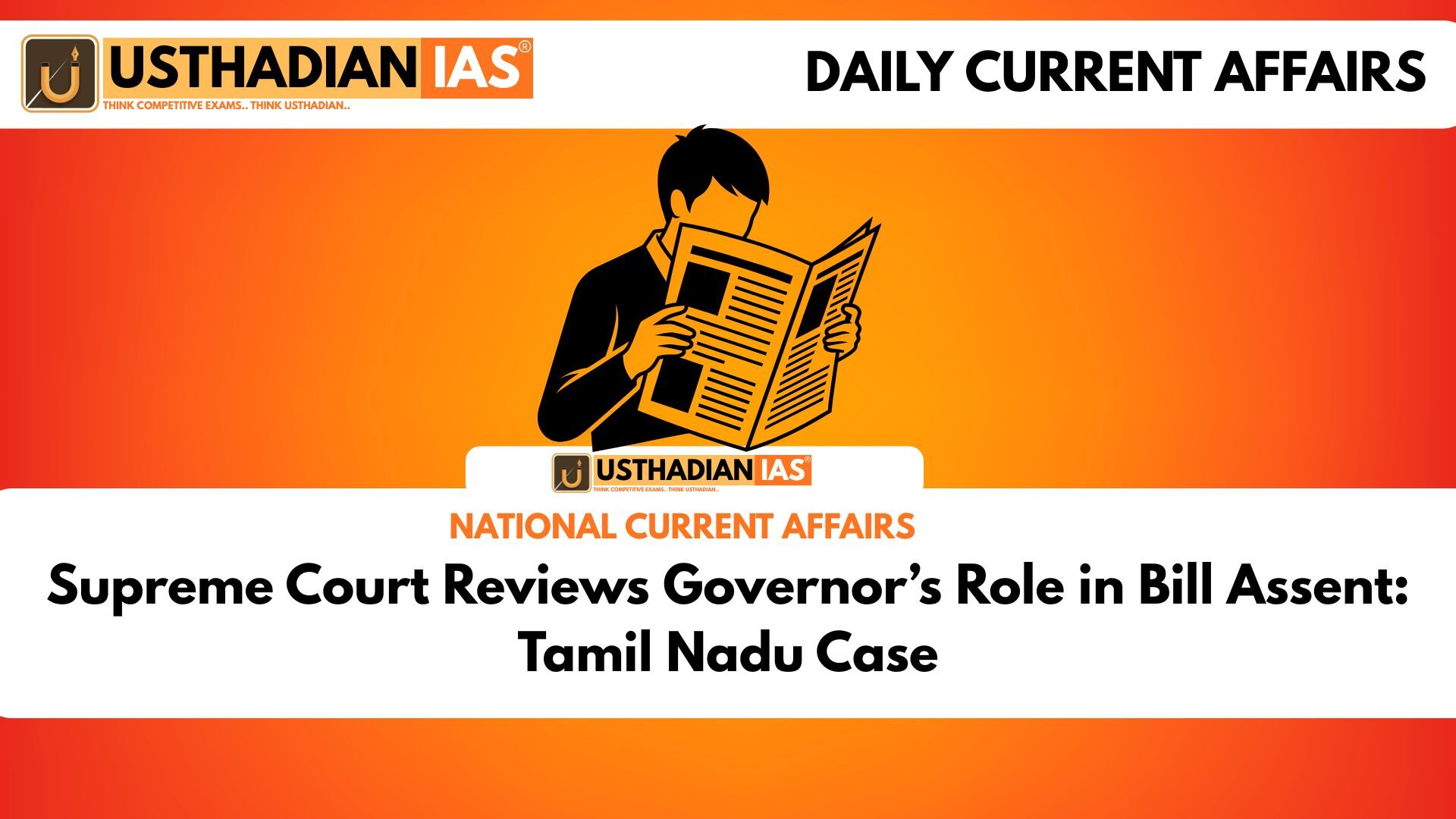संवैधानिक स्वीकृति पर कानूनी टकराव
भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक अहम संवैधानिक बहस चल रही है, जिसमें राज्यों के विधायी प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका पर विचार किया जा रहा है, विशेषकर जब वे किसी राज्य विधेयक को स्वीकृति देते हैं या रोकते हैं। यह मामला तमिलनाडु सरकार की याचिका से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राज्यपाल आर.एन. रवि ने कई विधेयकों पर लंबे समय तक कोई निर्णय नहीं लिया, जिससे राज्य की लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित हुई। यह मामला चुनी हुई राज्य सरकारों और केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपालों के बीच पुराने तनाव को उजागर करता है।
अनुच्छेद 200 पर बहस
इस विवाद का केंद्र भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 है, जो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की भूमिका को निर्धारित करता है। इसके अनुसार राज्यपाल के पास तीन विकल्प होते हैं:
- स्वीकृति देना,
- अस्वीकृति देना,
- राष्ट्रपति के पास आरक्षित करना।
यदि कोई विधेयक पुनः पारित किया जाता है, तो राज्यपाल को संवैधानिक रूप से उसे स्वीकृति देनी होती है, जब तक कि उसमें न्यायिक शक्ति का उल्लंघन न हो या वह असंवैधानिक न हो। हालांकि, इस अनुच्छेद में कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जिससे इसे “पॉकेट वीटो” कहा जाने लगा है—अर्थात् अनिश्चितकालीन विलंब।
तमिलनाडु में हालिया तनाव
सितंबर 2021 में आर.एन. रवि के राज्यपाल बनने के बाद से तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के बीच तनाव बढ़ा है। नवंबर 2023 में तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें कहा गया कि कई अहम विधेयक—जो शिक्षा, सामाजिक कल्याण, और प्रशासन से जुड़े हैं—2023 की शुरुआत से लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि राज्यपाल चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होते और उन्हें विधायी प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए।
न्यायालय में विचाराधीन मुख्य प्रश्न
सुप्रीम कोर्ट में जिन कानूनी मुद्दों की समीक्षा हो रही है, वे हैं:
- क्या विधानसभा द्वारा दोबारा पारित विधेयक को राज्यपाल अस्वीकृत कर सकते हैं?
- राष्ट्रपति को विधेयक भेजने की शक्ति क्या संवैधानिक सीमाओं के अधीन है?
- क्या विधेयक पर अनिश्चितकालीन देरी लोकतंत्र की भावना का उल्लंघन है?
- क्या राज्यपालों के लिए विधेयकों पर निर्णय लेने की समयसीमा निर्धारित की जानी चाहिए?
यह मामला भारतीय संघीय ढांचे में राज्य और केंद्र के बीच शक्ति–संतुलन को लेकर ऐतिहासिक निर्णय बन सकता है।
राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति
राज्यपाल किसी राज्य में सर्वोच्च संवैधानिक पद पर होते हैं और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि भी होते हैं। वे सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं, सिवाय कुछ मामलों के जैसे—राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना या कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति को भेजना।
राज्यपाल की शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ
कार्यपालिका शक्तियाँ: मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, राज्य चुनाव आयुक्त, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति। विश्वविद्यालयों के चांसलर के रूप में कार्य और राष्ट्रपति शासन की सिफारिश।
विधायी शक्तियाँ: विधानमंडल को बुलाना, स्थगित करना, भंग करना; विधेयक वापस भेजना (धन विधेयकों को छोड़कर), और अध्यादेश जारी करना।
वित्तीय शक्तियाँ: बजट की स्वीकृति, धन विधेयकों को पारित करना, आकस्मिक कोष से व्यय की अनुमति देना।
न्यायिक शक्तियाँ: राज्य अपराधों में क्षमादान, सजा में कमी; उच्च न्यायालय नियुक्तियों में परामर्श देना।
Static GK Snapshot
| विषय | विवरण |
| संविधानिक अनुच्छेद | अनुच्छेद 200 – राज्य विधेयकों पर राज्यपाल के विकल्प |
| मामला | तमिलनाडु बनाम राज्यपाल आर.एन. रवि |
| मुख्य कानूनी मुद्दा | विधेयकों की स्वीकृति में देरी |
| न्यायालय | भारत का सर्वोच्च न्यायालय |
| समीक्षा के अंतर्गत शक्ति | राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ |
| प्रमुख शब्द | पॉकेट वीटो – विधेयक पर अनिश्चितकालीन देरी |
| राज्य सरकार की दलील | देरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उल्लंघन |
| राज्यपाल की भूमिका | नाममात्र प्रमुख; मंत्रीमंडल की सलाह पर कार्य |
| संबंधित अनुच्छेद | अनुच्छेद 163 (मंत्रिपरिषद), अनुच्छेद 201 (राष्ट्रपति को आरक्षण) |
| संभावित प्रभाव | राज्यपाल की सीमाओं पर स्पष्टता, समयसीमा निर्धारण, संघीय संतुलन |