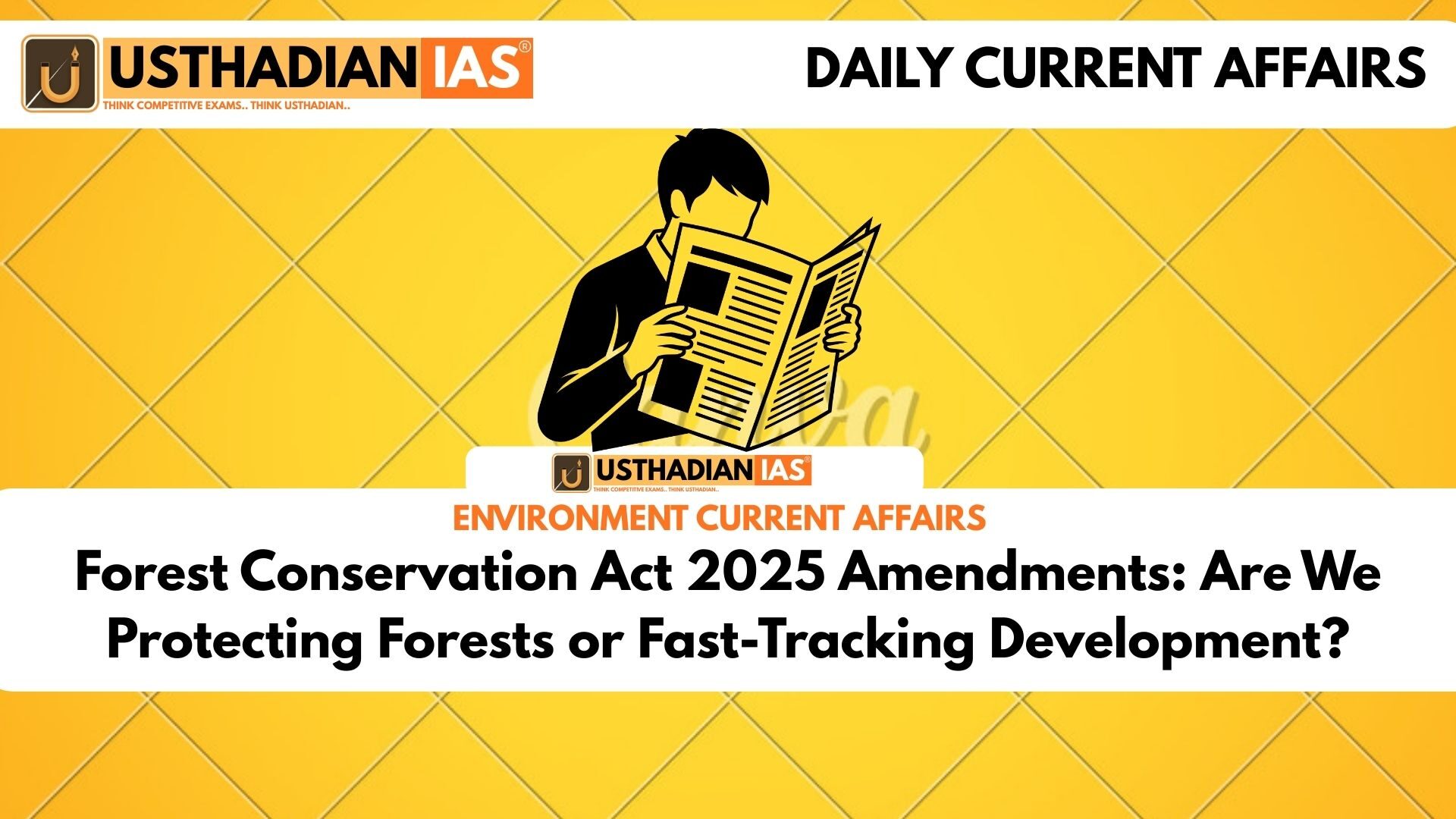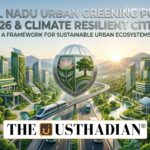क्या बदला गया और क्यों?
7 जनवरी 2025 को संसद ने वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में महत्वपूर्ण संशोधन पारित किए, जिससे यह तय किया गया कि अब केवल अधिसूचित या सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज भूमि को ही वन माना जाएगा। सरकार का तर्क है कि पुराना कानून आधुनिक बुनियादी ढांचे, सीमा सुरक्षा और आर्थिक विकास के अनुकूल नहीं था। लेकिन भारत का 24% क्षेत्रफल वन भूमि से ढका है—इसलिए हर संशोधन प्राकृतिक संसाधनों और कानून के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है।
सुप्रीम कोर्ट से संसद तक: 1996 का फैसला क्यों अहम था?
गोडावर्मन बनाम भारत संघ केस में 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्राकृतिक रूप से वन जैसी भूमि, भले ही अधिसूचित न हो, उसे भी वन संरक्षण के तहत माना जाए। इससे प्राइवेट जमीनें और बागान भी सरकारी नियंत्रण में आ गए। लेकिन 2025 संशोधन ने इस पर रोक लगा दी है। अब सिर्फ वे ही क्षेत्र वन माने जाएंगे जो आधिकारिक तौर पर अधिसूचित हों, जिससे किसानों और निजी जमीन मालिकों को कुछ राहत तो मिली, पर पर्यावरणीय जोखिम भी बढ़ा।
रणनीतिक परियोजनाओं को छूट—but at what cost?
संशोधन में कहा गया है कि सीमा से 100 किमी के भीतर या वामपंथी उग्रवाद (LWE) क्षेत्रों में रणनीतिक परियोजनाओं को कई पर्यावरणीय स्वीकृतियों से छूट दी जाएगी। इसका लाभ अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम जैसे राज्यों को मिलेगा। लेकिन कई राज्यों ने चिंता जताई है—मिजोरम को डर है कि यह वन विनाश को बढ़ावा देगा, सिक्किम चाहता है कि छूट क्षेत्र 2 किमी तक सीमित हो और छत्तीसगढ़ साफ परिभाषा की मांग कर रहा है।
क्या पेड़ लगाने से जंगल की भरपाई हो सकती है?
संशोधित कानून कहता है कि जब वन भूमि को साफ किया जाए, तो प्रतिपूरक वनीकरण (Compensatory Afforestation) जरूरी है। लेकिन अब यह निजी या खराब भूमि पर भी किया जा सकता है। इससे ग्रीन क्रेडिट और कॉर्पोरेट भूमि बैंकिंग को बढ़ावा मिल सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्राकृतिक वन की जगह युकलिप्टस जैसे मोनोकल्चर पेड़ लगाना जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की क्षति की भरपाई नहीं कर सकता।
क्या कार्यपालिका को मिल गई बहुत ज्यादा ताकत?
एक बड़ा विवाद इस बात को लेकर है कि अधिनियम में बहुत कुछ स्पष्ट नहीं है—बल्कि उसे पर्यावरण मंत्रालय के बनाए नियमों पर छोड़ा गया है। इससे कार्यपालिका (Executive) को अत्यधिक अधिकार मिलते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे सार्वजनिक निगरानी और न्यायिक चुनौती दोनों कठिन हो जाएंगी। राजनीति और शासन पढ़ने वाले छात्रों के लिए यह शक्ति पृथक्करण और पारदर्शिता पर एक गंभीर प्रश्न है।
STATIC GK SNAPSHOT FOR COMPETITIVE EXAMS
| विषय | तथ्य |
| मूल वन अधिनियम वर्ष | 1980 में पारित |
| महत्वपूर्ण न्यायिक मामला | टी.एन. गोडावर्मन बनाम भारत संघ (सुप्रीम कोर्ट, 1996) |
| 2025 संशोधन का केंद्रबिंदु | केवल अधिसूचित/दर्ज वन भूमि पर लागू |
| सीमा छूट क्षेत्र | 100 किमी (रणनीतिक परियोजनाओं के लिए) |
| विरोध करने वाले राज्य | मिजोरम, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ |
| नया वनीकरण नियम | निजी या क्षरणयुक्त भूमि पर वनीकरण की अनुमति |
| रणनीतिक परियोजना की परिभाषा | स्पष्ट नहीं; पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बाद में तय की जाएगी |
| मुख्य चिंता | कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि और पर्यावरणीय जोखिम |
| भारत का वन क्षेत्र (2023-24) | कुल भू-भाग का लगभग 24% |