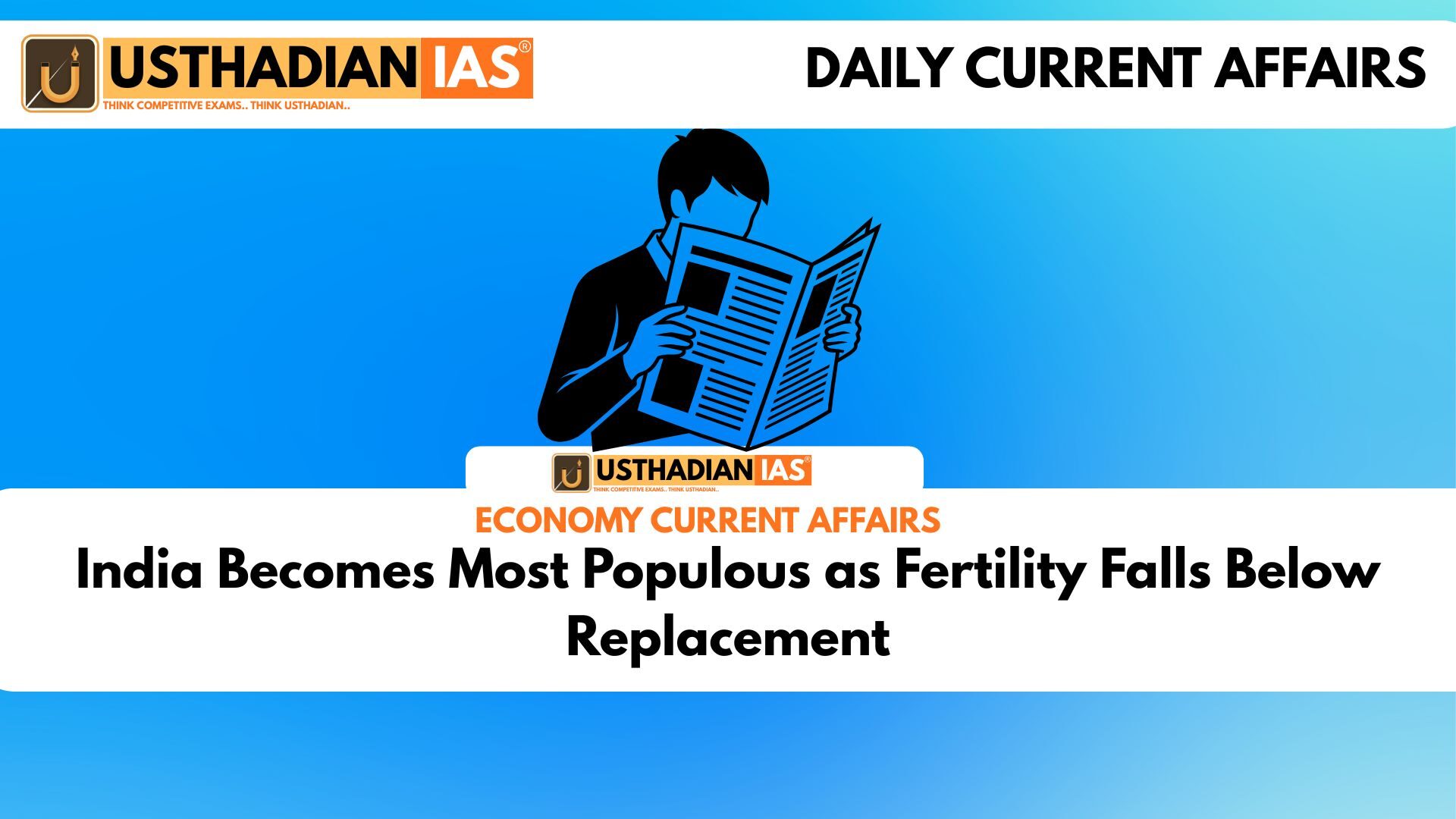चालू घटनाएँ: भारत की जनसंख्या 2025, UNFPA प्रजनन रिपोर्ट, कुल प्रजनन दर भारत, जनसांख्यिकीय लाभांश, विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2025, भारत की जनसंख्या चोटी 2064, बुजुर्गों की वृद्धि, भारत में जीवन प्रत्याशा 2025, भारत की युवा जनसंख्या, भारत में प्रजनन स्वास्थ्य
भारत ने जनसंख्या की ऐतिहासिक सीमा पार की
भारत की जनसंख्या वर्ष 2025 में आधिकारिक रूप से 1.46 अरब तक पहुँच गई है, जिससे भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। यह केवल आँकड़ों की बात नहीं है, बल्कि यह सामाजिक बदलाव, घटती प्रजनन दर और बढ़ती जीवन प्रत्याशा को दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) के अनुसार, भारत की जनसंख्या लगभग 2060 के दशक की शुरुआत में 1.7 अरब पर पहुँचकर धीरे-धीरे कम होने लगेगी।
प्रतिस्थापन स्तर से नीचे पहुंची प्रजनन दर
रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) अब 1.9 बच्चों प्रति महिला है, जो कि प्रत्यावर्तन स्तर 2.1 से कम है। इसका अर्थ है कि औसतन भारतीय महिलाएं अब इतनी संतानें नहीं जन्म दे रही हैं जिससे अगली पीढ़ी की जनसंख्या स्थिर बनी रह सके। यह बदलाव अचानक नहीं हुआ, बल्कि यह शिक्षा, सामाजिक सुधार और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर उपलब्धता का परिणाम है।
संयुक्त राष्ट्र की दृष्टि से प्रजनन में बदलाव
UNFPA की 2025 की ‘स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट‘ जिसका शीर्षक है “द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस“, यह बताती है कि घटती प्रजनन दर को लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय, फोकस इस पर होना चाहिए कि लोग अपनी पसंद के अनुसार परिवार नियोजन कर सकें, उन्हें सभी जानकारी और संसाधन उपलब्ध हों, और महिलाओं एवं परिवारों को सहयोग देने वाली नीतियाँ बनें।
भारत की जनसंख्या संरचना में बदलाव
भारत की जनसांख्यिकीय संरचना यह दर्शाती है कि देश बदलाव के दौर में है:
- 0–14 वर्ष के आयु वर्ग में 24%
- 10–19 वर्ष में 17%
- 10–24 वर्ष के युवा 26%
- 15–64 वर्ष के कामकाजी आयु वर्ग में 68%
यह भारत के लिए जनसांख्यिकीय लाभांश का स्वर्णिम अवसर है। यदि रोजगार, कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियाँ मजबूत हों, तो यह जनसंख्या भारत की आर्थिक प्रगति में अहम भूमिका निभा सकती है।
जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और बुजुर्गों की संख्या में इज़ाफ़ा
प्रजनन दर में गिरावट के साथ-साथ जीवन प्रत्याशा भी बढ़ी है। 2025 में भारतीय पुरुषों की औसत आयु 71 वर्ष और महिलाओं की 74 वर्ष हो गई है। इस कारण बुजुर्ग जनसंख्या (65 वर्ष से अधिक) अब 7% है और भविष्य में यह तेजी से बढ़ेगी। इसके चलते बुजुर्गों की देखभाल, पेंशन योजनाओं और स्वास्थ्य ढांचे में सुधार की आवश्यकता होगी।
भारत यहाँ तक कैसे पहुँचा?
1960 के दशक में भारतीय महिलाओं के औसतन 6 बच्चे होते थे और भारत की जनसंख्या लगभग 436 मिलियन थी। उस समय गर्भनिरोधक का प्रचलन बहुत कम था और लड़कियों की शिक्षा सीमित थी। आज स्थिति काफी बदल चुकी है:
- लड़कियों की शिक्षा दर में वृद्धि
- स्वास्थ्य सेवाओं और परिवार नियोजन की पहुँच बेहतर
- महिलाओं की निर्णय लेने में भागीदारी बढ़ी
आज अधिकांश महिलाएं औसतन दो बच्चे ही जन्म दे रही हैं, जो कि एक ऐतिहासिक बदलाव है।
अब भी चुनौतियाँ शेष हैं
इन उपलब्धियों के बावजूद, आज भी कई महिलाएं पूरी तरह से अपनी प्रजनन पसंदों पर नियंत्रण नहीं रख पाती हैं, खासकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में। राज्य और समुदायों के बीच असमानताएँ अभी भी व्यापक हैं। आगे का रास्ता यही होना चाहिए कि हर महिला को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के अधिकार और संसाधन उपलब्ध हों।
एक आशावादी भविष्य
UNFPA की भारत प्रतिनिधि एंड्रिया एम. वोजनर के अनुसार, भारत की यह प्रगति दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और जनसंख्या में बदलाव के साथ, भारत प्रजनन अधिकारों और आर्थिक विकास को जोड़ने वाला वैश्विक नेतृत्वकर्ता बन सकता है।
Static Usthadian Current Affairs Table
| विषय | विवरण |
| भारत की जनसंख्या (2025) | 1.46 अरब |
| अनुमानित अधिकतम जनसंख्या | 1.7 अरब (2060 के दशक की शुरुआत) |
| कुल प्रजनन दर (TFR) | 1.9 बच्चे प्रति महिला |
| प्रतिस्थापन प्रजनन दर | 2.1 |
| जीवन प्रत्याशा (पुरुष) | 71 वर्ष |
| जीवन प्रत्याशा (महिला) | 74 वर्ष |
| कामकाजी आयु वर्ग (15–64) | 68% |
| बुजुर्ग जनसंख्या (65+) | 7% |
| बालिकाओं की शिक्षा का प्रभाव | स्कूल उपस्थिति में वृद्धि |
| UNFPA रिपोर्ट का शीर्षक | द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस |
| रिपोर्ट जारी करने वाला संगठन | संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) |
| भारत की जनसंख्या (1960) | 436 मिलियन |
| प्रजनन दर (1960) | लगभग 6 बच्चे प्रति महिला |
| प्रमुख जनसांख्यिकीय वर्ग | युवा (10–24 वर्ष): 26% |
| वृद्धावस्था प्रवृत्ति | तीव्र वृद्ध जनसंख्या वृद्धि |