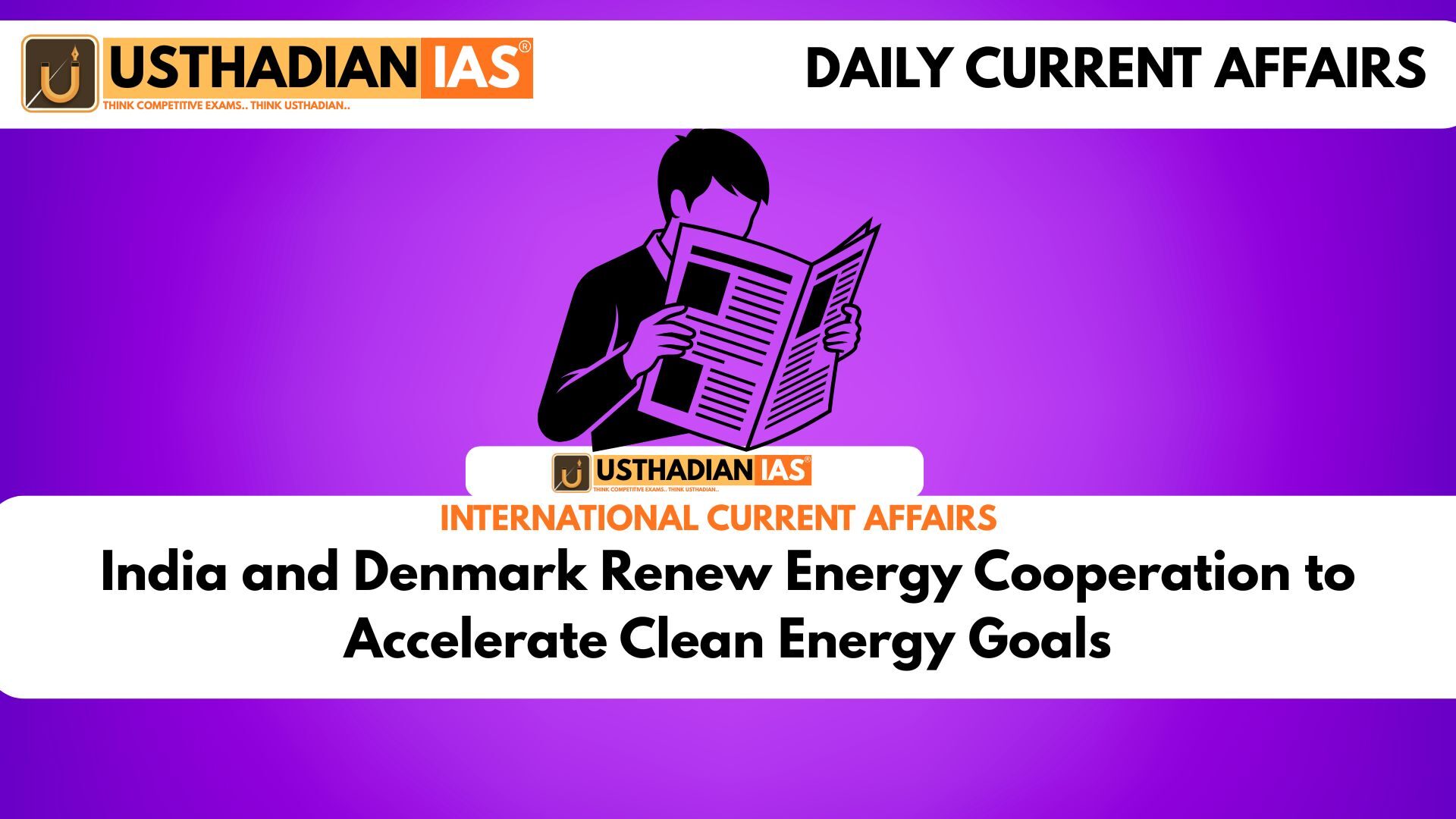यह समझौता क्यों है समयोचित और महत्वपूर्ण
जलवायु परिवर्तन और स्थिरता पर बढ़ते वैश्विक ध्यान के बीच, भारत और डेनमार्क ने 2 मई 2025 को स्वच्छ ऊर्जा सहयोग को पुनः सशक्त करने हेतु नई समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता भारत के ऊर्जा मंत्रालय के सचिव श्री पंकज अग्रवाल और भारत में डेनमार्क के राजदूत श्री रासमस एबिलगार्ड क्रिस्टेन्सन के बीच संपन्न हुआ। यह साझेदारी भारत के 2070 तक नेट–ज़ीरो उत्सर्जन के दीर्घकालिक लक्ष्य को प्रत्यक्ष रूप से समर्थन देती है।
हरित सहयोग की मज़बूत नींव पर आधारित
यह समझौता कोई नया आरंभ नहीं बल्कि जून 2020 में शुरू हुई पांच वर्षीय साझेदारी का नवीनीकरण है। इस अवधि में दोनों देशों ने ऊर्जा क्षेत्र में तकनीक और ज्ञान साझेदारी पर गहराई से काम किया है। डेनमार्क की विशेषज्ञता पवन ऊर्जा, ग्रिड इंटीग्रेशन और लो–कार्बन तकनीकों में है, जिससे यह भारत के हरित ऊर्जा अभियान में एक रणनीतिक सहयोगी बन गया है।
प्राथमिकता वाले क्षेत्र: पावर मॉडलिंग से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तक
यह MoU विस्तृत और दूरदर्शी क्षेत्र को कवर करता है। इसमें शामिल हैं:
- पावर सिस्टम मॉडलिंग, जिससे भारत भविष्य की ऊर्जा मांगों का पूर्वानुमान लगा सके
- सौर एवं पवन जैसी परिवर्तनीय अक्षय ऊर्जा को राष्ट्रीय ग्रिड में समाहित करना
- ईवी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास
- सीमा–पार विद्युत व्यापार जैसे क्षेत्र, जो ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग के लिए अहम हैं
यह समझौता भारत को आधुनिक, भविष्य–उन्मुख ऊर्जा प्रणालियों की ओर ले जाता है।
नवाचार के लिए ज्ञान साझा करना
समझौते का एक विशेष पहलू ज्ञान हस्तांतरण और क्षमतावृद्धि पर बल है। इसके तहत संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम, विशेषज्ञ बैठकों और अध्ययन यात्राओं का आयोजन होगा, जिससे दोनों देशों के ऊर्जा पेशेवरों को वास्तविक नवाचारों का प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा। इससे दीर्घकालिक सहयोग की नींव मजबूत होगी, और डेनमार्क की विशेषज्ञता भारत के नीति और स्केल से जुड़कर ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव लाएगी।
Static GK परीक्षा-संक्षेप सारणी
| विषय | विवरण |
| समझौता हस्ताक्षर तिथि | 2 मई 2025 |
| समझौते का प्रकार | नवीनीकृत समझौता ज्ञापन (MoU) |
| भारतीय प्रतिनिधि | श्री पंकज अग्रवाल (सचिव, विद्युत मंत्रालय) |
| डेनिश प्रतिनिधि | श्री रासमस एबिलगार्ड क्रिस्टेन्सन (भारत में डेनमार्क के राजदूत) |
| प्रारंभिक समझौता वर्ष | जून 2020 |
| भारत का जलवायु लक्ष्य | 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन |
| प्रमुख फोकस क्षेत्र | पावर सिस्टम मॉडलिंग, अक्षय ऊर्जा एकीकरण, ईवी चार्जिंग अवसंरचना |
| ज्ञान साझेदारी उपकरण | संयुक्त प्रशिक्षण, विशेषज्ञ बैठकें, अध्ययन यात्राएं |
| व्यापक उद्देश्य | तीव्र स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और सतत विकास |