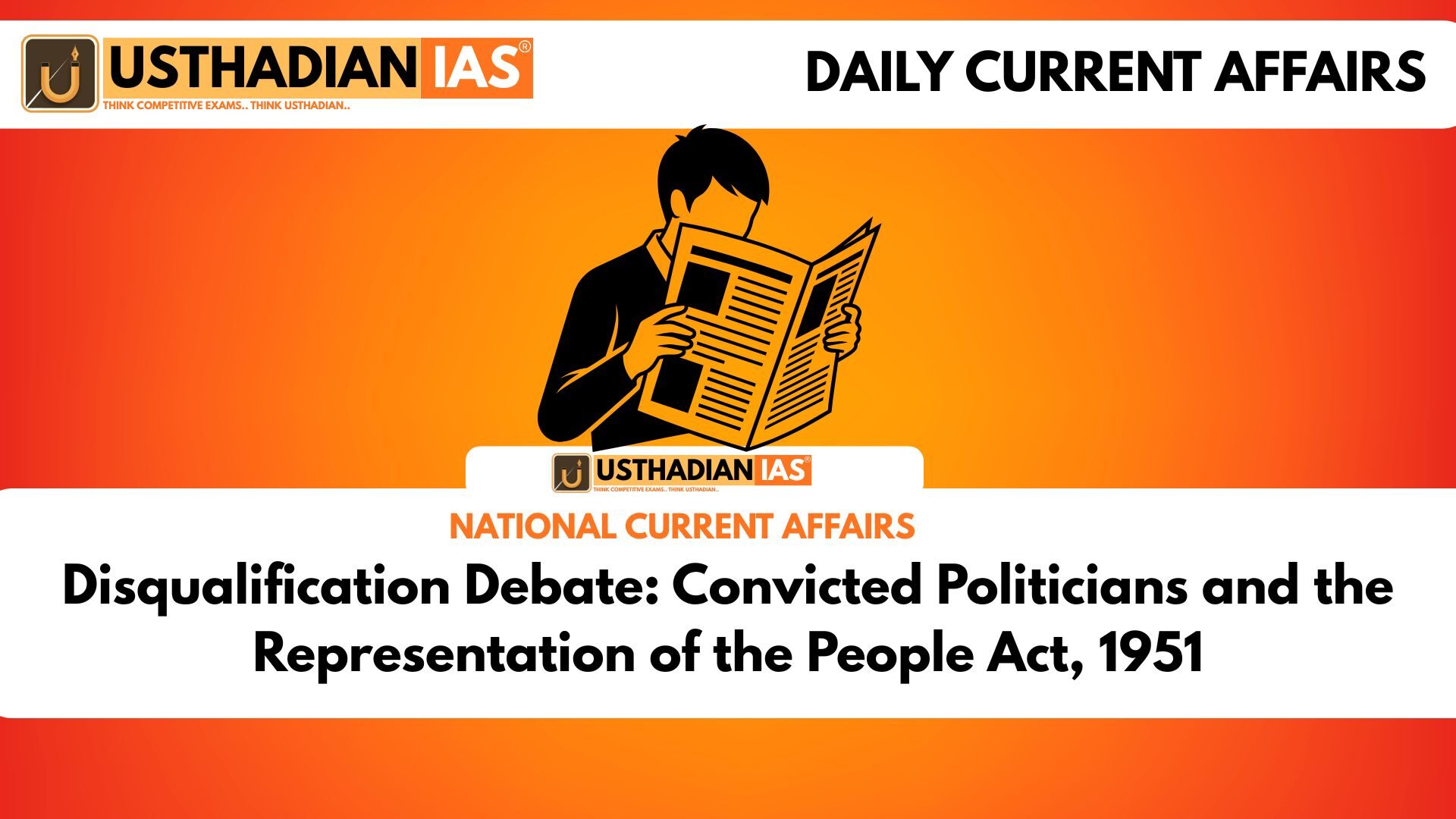कानून की पृष्ठभूमि
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 भारत की चुनावी व्यवस्था की मूल आधारशिला है। यह कानून न केवल चुनाव संचालन के नियम तय करता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि कौन व्यक्ति चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होता। विशेष रूप से, धारा 8 के तहत, कुछ अपराधों में दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को जेल से रिहा होने के बाद छह वर्षों तक अयोग्य माना जाता है। वहीं धारा 9 उन लोक सेवकों पर पांच वर्ष का प्रतिबंध लगाती है जिन्हें भ्रष्टाचार या विश्वासघात के लिए बर्खास्त किया गया हो। ये समय–सीमित दंड भविष्य में सुधार की संभावना बनाए रखते हुए निवारक के रूप में कार्य करते हैं।
छह साल के प्रतिबंध का सरकार का पक्ष
हाल ही में केंद्र सरकार ने अदालत में यह रुख दोहराया कि छह साल की अयोग्यता की अवधि संविधान–सम्मत और उचित है। सरकार का कहना है कि दुनिया के कई दंड विधानों में इसी प्रकार के समयबद्ध प्रतिबंध होते हैं, जो निवारक होते हैं लेकिन अत्यधिक कठोर नहीं। इसके साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंध की अवधि तय करना संसद का अधिकार क्षेत्र है, न कि न्यायपालिका का।
याचिकाकर्ता की मांग: आजीवन प्रतिबंध
वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में दोषी राजनेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। उनका तर्क है कि छह वर्ष के बाद राजनीति में वापसी की अनुमति चुनावी नैतिकता को कमज़ोर करती है। उनका मानना है कि इससे अपराध और राजनीति का चक्र बना रहता है, जो जन विश्वास और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाता है।
न्यायिक समीक्षा बनाम विधायी अधिकार
इस बहस का मूल सवाल है: विधायी अधिकार कहां समाप्त होता है और न्यायिक समीक्षा कहां शुरू होती है? सरकार का कहना है कि कानूनों की समीक्षा अदालत कर सकती है, लेकिन विधायिका की नीति–निर्धारण प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यदि आजीवन प्रतिबंध की व्यवस्था लानी है, तो यह संसद के माध्यम से ही कानून में संशोधन द्वारा किया जाना चाहिए, न कि न्यायिक आदेश द्वारा।
संवैधानिक और व्यावहारिक प्रभाव
यह मुद्दा संवैधानिक संतुलन का प्रतीक है—एक ओर चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करना, दूसरी ओर सुधार के अवसर देना। आजीवन प्रतिबंध को अत्यधिक दंडात्मक माना जा सकता है, जबकि छोटे प्रतिबंध अवधि से अपराधियों की शीघ्र राजनीतिक वापसी जनता का भरोसा तोड़ सकती है। इस संतुलन को विधायी और न्यायिक दोनों दृष्टिकोण से सोचने की आवश्यकता है।
STATIC GK SNAPSHOT – प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जानकारी सारांश
| विषय | तथ्य |
| अयोग्यता संबंधित कानून | जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 |
| दोष सिद्धि पर प्रतिबंध | धारा 8 – रिहाई के बाद 6 वर्ष तक अयोग्यता |
| लोक सेवकों पर प्रतिबंध | धारा 9 – भ्रष्टाचार/विश्वासघात पर 5 वर्ष का प्रतिबंध |
| याचिका दायरकर्ता | अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय |
| सरकार का वर्तमान रुख | 6 वर्ष का प्रतिबंध उचित और संवैधानिक |
| प्रस्तावित परिवर्तन | दोषी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध |
| न्यायपालिका की भूमिका | समीक्षा कर सकती है, पर निर्णय संसद का विषय |
| संबंधित संवैधानिक सिद्धांत | विधायी मंशा बनाम न्यायिक समीक्षा का संतुलन |